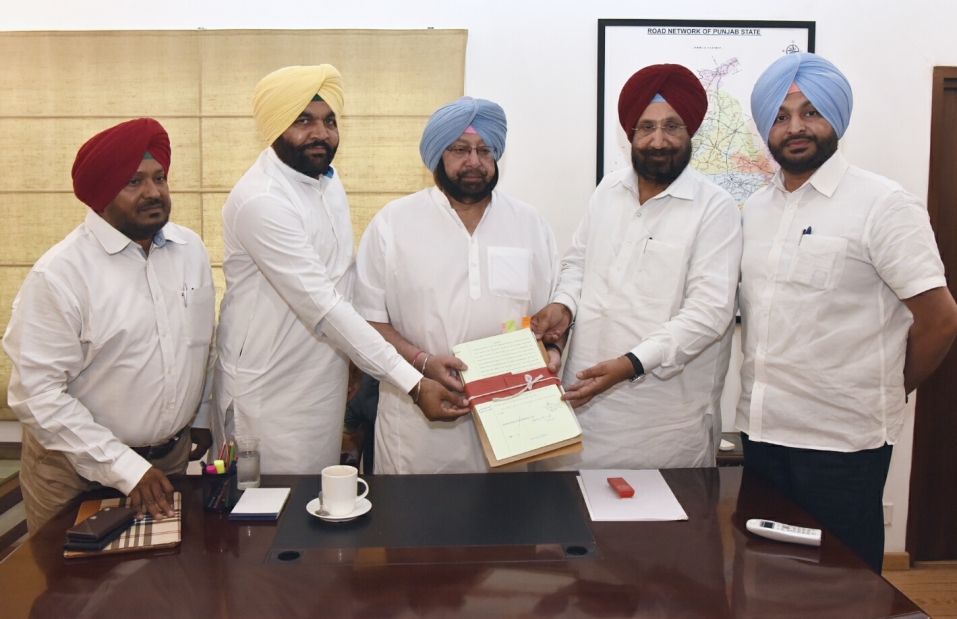जीवन में भाग्य की भूमिका

मनुष्य के जीवन में भाग्य की भूमिका के बारे में सदा से ही एक गंभीर बहस चलती आ रही है। विचारकों के एक वर्ग का दावा है कि भाग्य सब कुछ नियंत्रित करता है । इस दर्शन के समर्थकों का मानना है कि भगवान ने पहले से ही हर किसी के लिए सब कुछ तय कर रखा है , और मनुष्य उसके लिए पहले से तैयार किए गए पथ पर चलने के लिए बाध्य है। इन भाग्यवादियों के अनुसार , किसी को भी अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता नहीं है ।
दूसरी ओर , जो लोग स्वतंत्र इच्छाशक्ति के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, वे दावा करते हैं कि नियति नाम की कोई चीज नहीं होती । वे इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किसी की परिस्थितियां और उस की सफलताएं एवं असफलताएं उसकी अपनी बनाई हुई होती हैं। दोनों ओर के विचारकों के अपने-अपने तर्क हैं ।
भगवद् गीता के श्लोक संख्या 18.13 से 18.15 में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। किसी भी कार्य की सिद्धि में निम्मलिखित पांच कारक बताए गए हैं :(1) अधिष्ठान (2) कर्ता (3) उपकरण (4) चेष्टा ; और (5) दैव । जो भी उचित या अनुचित कर्म व्यक्ति अपने शरीर , वाणी या मन के द्वारा करता है – वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप ही होता है । दूसरे शब्दों में, ये पांच कारण ही किसी कार्य की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं।
प्रथम घटक अर्थात् अधिष्ठान का शाब्दिक अर्थ है निवास । यहां यह शरीर को संदर्भित करता है, क्योंकि यही सब क्रियाओं का आधार है । शरीर ही वह स्थान है जहां से सभी क्रियाएं होती हैं । दूसरे घटक अर्थात् कर्ता का अर्थ होता है , कार्य को करने वाला। कर्ता यहां अहं को संदर्भित करता हैं क्योंकि वही है जो सभी कर्म करता है। केवल एक साक्षी होने के कारण , आत्मा तो अकर्ता है। परन्तु आत्मा को भी क्रिया के निर्धारक कारणों में शामिल किया जा सकता है क्योंकि आत्मा की चेतना के बिना अहं कोई गतिविधि नहीं कर सकता । तीसरे घटक अर्थात् उपकरण का अर्थ होता है साधन । कर्म के विभिन्न प्रकार के साधन हैं इन्द्रियां वगैरह। इन सभी कारकों के माध्यम से ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है।
ये तीनों घटक अर्थात् शरीर, अहं (या आत्मा ) और इन्द्रियॉं वगैरह प्रकृति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि किसी का भी अपने जन्म पर नियंत्रण नहीं होता है। कोई कब, कहां और किन हालात में पैदा होगा , यह कोई तय नहीं कर सकता । वह अपने वंश, सामाजिक परिवेश या आर्थिक स्थिति आदि का चयन नहीं कर सकता । ये सब तो जीवात्मा के संचित कर्मों और विभिन्न अन्य परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं, जो कि वर्तमान में व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हैं।
जीवन की उपर्युक्त तीन सम्पदाओं को बदला नहीं जा सकता । परन्तु इन सीमाओं के भीतर रहते हुए , मनुष्य को अपनी राह स्वयं चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। यही कारण है कि किसी कार्य की सिद्धि में शामिल चौथा कारक अर्थात् चेष्टा अति महत्वपूर्ण होता है । यह मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयासों को दर्शाता है । इमानदार प्रयासों के द्वारा व्यक्ति विपरित परिस्थितियों से भी पार पा सकता है ।
यहां पर यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि चेष्टा का तात्पर्य किसी भी प्रकार के प्रयास से नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए उचित प्रयासों से है ।कार्य की स्वतंत्रता का उपयोग स्वयं को नष्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिये । यही वजह है कि अर्जुन के साथ अपने संवाद के अन्त में श्रीकृष्ण ने उसे सलाह दी कि वह उसे दिए गए ज्ञान के बारे में गंभीरता से विचार करे और फिर तय करे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है ।
इस प्रकार, भगवद् गीता इस विचार का समर्थन नहीं करती कि जो होना तय है वह निश्चित रूप से होगा ही। यदि ऐसा होता,तो कार्य की सिद्धि में चेष्टा की कोई भूमिका नहीं होती । एक उदाहरण के तौर पर ताश के खेल में एक खिलाड़ी ने न ही खेल का आविष्कार किया है और न ही उस ने खेलने के नियमों को बनाया है । वह यह भी तय नहीं कर सकता कि उसे कौन से पत्ते मिलेंगे। इस हद तक उसके पास चुनने का कोई अधिकार नहीं है । लेकिन खेल को अच्छे या बुरे ढ़ंग से खेलना तो उसके अपने ही हाथ में है। एक अच्छा खिलाड़ी सबसे खराब पत्तों के साथ भी जीत सकता है , और बुरा खिलाड़ी बहुत अच्छे पत्तों के बावजूद भी हार जाता है । इसी उदाहरण को व्यापक परिपेक्ष्य में देखें तो ईश्वर ने मानव जाति को विभिन्न समर्थन प्रणालियों के रूप में संपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान कर दी है । अब मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह खुद को बनाता है या बिगाड़ता है।
सफलता केवल कड़ी मेहनत से सुनिश्चित नहीं होती । सभी मानवीय प्रयासों में हमेशा एक अलौकिक तत्व मौजूद रहता है जो उस प्रयास में सफलता या विफलता की संभावना को बढ़ाता या कम करता है । कभी-कभी मनुष्य को अनुकूल परिस्थितियों और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वॉंछित परिणाम नहीं मिलता । और कभी-कभी वह बिना ज्यादा मेहनत के भी आशा से अधिक फल प्राप्त कर लेता है । यही कारण है कि किसी कार्य की सिद्धि के कारकों में से एक दैव यानी परमात्मा का विधान बताया गया है । इस अज्ञात कारक को अक्सर भाग्य कहा जाता है । किसी के भी जीवन में भाग्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । भाग्य का अपना महत्व है । परन्तु नियति में विश्वास कभी भी निष्क्रियता या लापरवाही का बहाना नहीं होना चाहिये ।
निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि निष्ठापूर्वक कार्य और दैवीय कृपा दोनों ही किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रयास और सौभाग्य एक दूसरे से अलग नहीं हैं । इस प्रकार , मनुष्य को दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए ; और फिर सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिये । परमेश्वर किसी संकीर्ण विचार के लिए नहीं बल्कि एक व्यापक और उच्च उद्देश्य के साथ कार्य करता है; जिसको मनुष्य कभी समझ पाता है और कभी नहीं समझ पाता ।