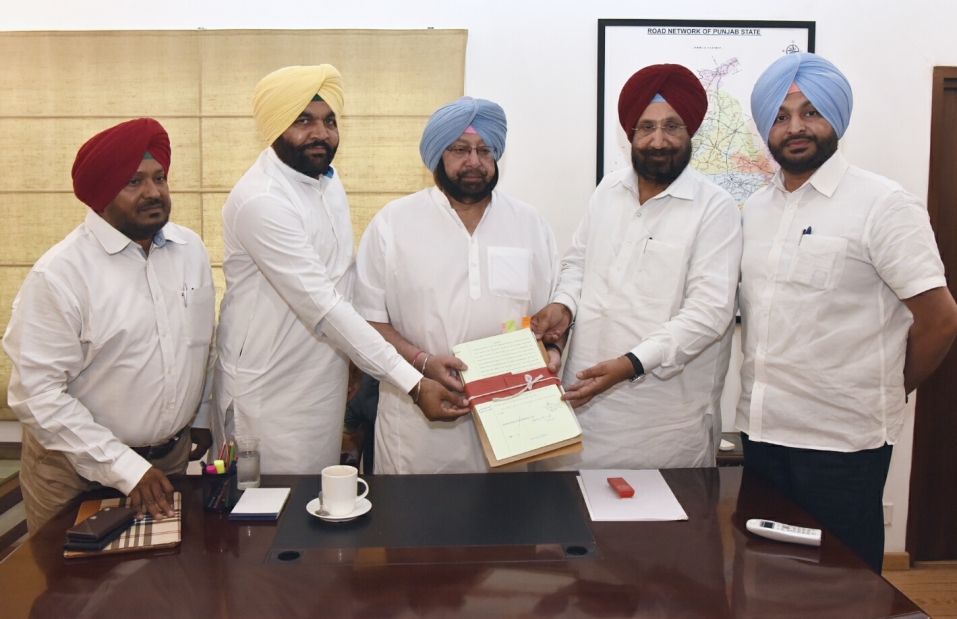केरल विनाश में हम दूसरों से क्यों नहीं सीख सकते?

बीस साल पहले अगस्त 1998 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री झू रोंगजी ने चीन की स्टेट काउंसिल की एक बैठक में सिचुआन प्रांत की जंगली ढलानों वाले इलाकों में पेड़ काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था। यह विनाशकारी बाढ़ संकट के जवाब में था, जिसका सामना चीन यांग्त्जी नदी बेसिन के बढ़े जल स्तर के कारण कर रहा था।
उस नीति को रातोंरात अधिनियमित किया गया था, जबकि यांग्त्जी नदी में बाढ़ अभी भी अपने चरम पर था और बचाव अभियान जोरों पर था। यह जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल के सिर्फ एक साल बाद आया था, लेकिन झू इस बात को लेकर विश्लेषण करने के मूड में नहीं थे कि क्या यह विनाशकारी घटना जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है।
उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यांग्त्जी नदी में कुछ इसी तरह की बाढ़ 1870, 1931 और 1954 में आई थी। उस पर जलवायु परिवर्तन की समस्या नहीं थी। झू ने उसी बैठक में वनों की कटाई पर गंभीर दंड की घोषणा की और 2000 व 2010 तक के लिए महात्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ वनरोपण को प्रोत्साहित किया।
ठीक उसी महीने में लेकिन अब 2018 में भारत केरल में विनाश का सामना कर रहा है, जो 1924 के बाद से सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में है। 400 से अधिक लोगों की मौत और दस लाख बेघरों के साथ यह सवाल उठता है कि बांधों के बाढ़ द्वार से पानी को छोड़ा जाना और इसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति को सही से नहीं संभाल पाना क्या एक प्राकृतिक या मानवीय भूल की वजह से उत्पन्न हुई आपदा है? क्या यह जलवायु घटना है या ग्लोबल वार्मिग के कारण है?
जलवायु परिवर्तन में कारक श्रृंखला को जोड़ने के लिए यह आसान और सुविधाजनक है। दरअसल, ग्लोबल वार्मिग से समुद्र और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हुई है (पूर्व-औद्योगिक समय पर लगभग एक डिग्री सेल्सियस) जिसके परिणामस्वरूप पिछले छह दशकों में मौसम की घटनाओं में बड़े उलटफेर में वृद्धि हुई है।
एक सीमा तक, ग्लोबल वार्मिग वास्तव में भारी बारिश के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह 'चरम' और 'स्थानीय' वर्षा को स्पष्ट नहीं करता है। अप्रत्याशित वर्षा को रोका नहीं जा सका, चाहे यह ग्लोबल वार्मिग के कारण हो या नहीं, लेकिन जो तबाही हुई उसे नियंत्रित किया जा सकता था।
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल में अंधाधुंध वनों की कटाई ने 1920 से 1990 के बीच वनों को 40 प्रतिशत कम कर दिया है। 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिपोर्ट' के मुताबिक, 1973 और 2016 के बीच लगभग दस लाख हेक्टेयर वन भूमि समाप्त हो चुकी है। इसने दलदल, जमीन धंसने जैसी घटनाओं पर काबू करने की मिट्टी की क्षमता को कम कर दिया गया है। अवैध खनन, जिसमें बाढ़ के पानी 'बाढ़' के रेत और पत्थर शामिल हैं, केरल में जोरों पर हैं। अत्यधिक उत्साही जल पर्यटन ने बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाकों के बाढ़ के पानी का सामना नहीं कर पाने जैसी कमजोरी को उजागर होने दिया। असंगठित बांध-जल प्रबंधन ने समुदायों और वन्यजीवों को अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से बचाने के लिए मझधार में छोड़ दिया।
क्या कोई रास्ता है?
सीखने और इसका हिस्सा बनने के कई उदाहरण और पहल हैं। नासा और जापान एयरोस्पेस एजेंसी के ग्लोबल वर्षा मापन (जीपीएम) विज्ञान ने कुछ दिन पहले ही केरल बाढ़ को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। जीपीएम के साथ सहयोग और आपदा प्रबंधन उपायों को समय पर शुरू कर देने से तबाही को रोकने में मदद मिल जाती।
स्विट्जरलैंड (लगभग केरल के समान आकार का) में केरल के 61 बांधों के मुकाबले 200 बड़े बांध हैं। स्विट्जरलैंड के प्राधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण सुरक्षा और बाढ़ द्वार के संचालन का समन्वय करता है। इस तरह के बांध प्रबंधन और जलप्लावन-मापन पर स्विट्जरलैंड के साथ सहयोग करना भारत को भविष्य के लिए तैयार करेगा। केरल में, इसके 61 में से किसी भी बांध के लिए सुरक्षा विश्लेषण नहीं किया गया था।
चीन ने अब आपदा एवं बाढ़ प्रबंधन में बड़ा अनुभव हासिल किया है। मानव इतिहास में पांच सबसे भयावह बाढ़ चीन में आए हैं। चीन के साथ सहयोग करने से भारत को बाढ़ क्षति से निपटने और इसका प्रबंधन करने में काफी मदद मिलेगी।
(लेखक टेरे पॉलिसी सेंटर के चेयरमैन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के पूर्व निदेशक हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके अपने निजी विचार हैं)