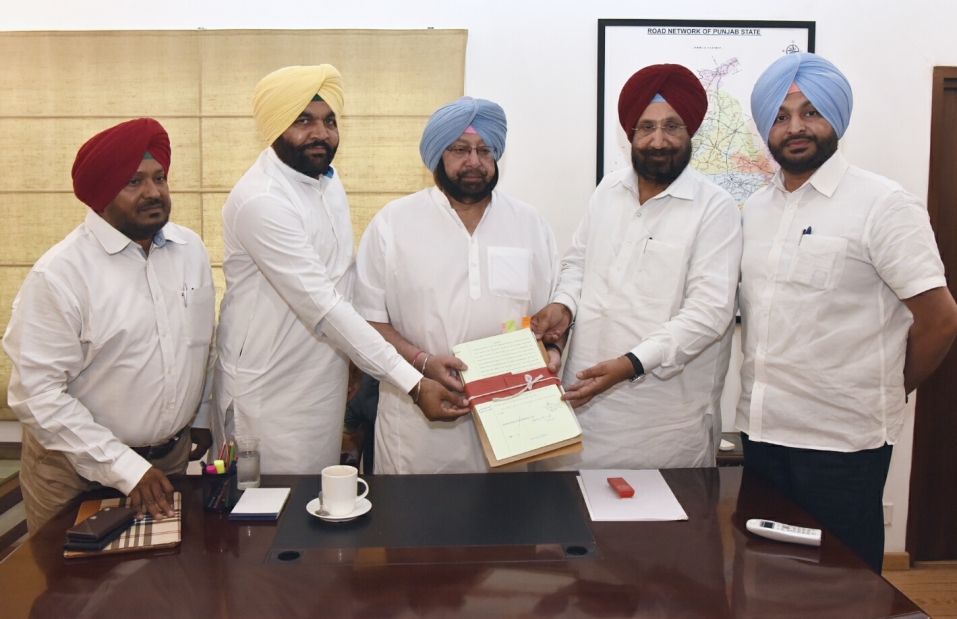योग शुरू करने से पहले जाने ये बाते
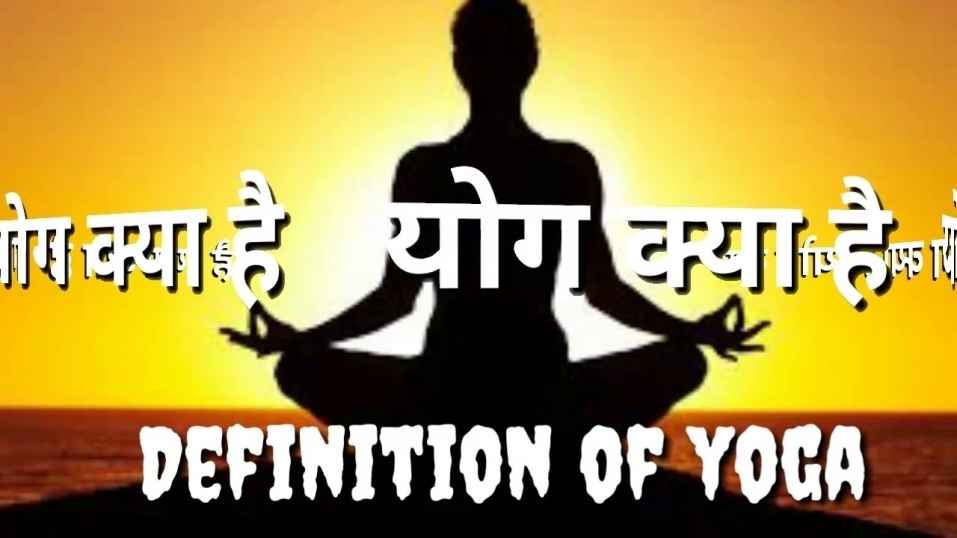
| डॉ सुभा कौशल |
योग का शाब्दिक अर्थ है- जोड़ना , दो का एक होना । शरीर , मन एवं आत्मा का एकीकार होने को योग कहते है। शरीर और मन का आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाना योग कहलाता है। वह साधन जिसके द्वारा साधक विषयों का सेवन करते हुए भी जले कमलवत निर्लिप्त रह सकता है । आसक्ति का त्याग कर नियत कर्मों की ओर अग्रसर होना ही योग है । मन की वृति की एकाग्रता ही योग है । योग तत्वत; एक सूक्ष्म विजान पर आधारित आध्यात्मिक विषय है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करवाता है । भौतिक स्तर पर यह स्वस्थ जीवन जीने की कला है एवं आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति की चेतना ब्रह्राण्ड की चेतना से जुड़ जाती है । जो प्रकृति के परिपूर्ण सामंजस्य का घोतक है ।
योग का इतिहास
योग विद्या को सप्तऋषियों को दिया गया जिनसे यह अन्य ऋषि- मुनियों तपस्वियों तक पहुंचा । फिर कृष्ण ,महावीर व बुद्व द्वारा इस पद्वति को नया आयाम प्राप्त हुआ । इसके बाद योग को पतंजलि ने स्थापित किया । जैन और बौद्व काल में यम-नियम पर बल दिया गया । अहिंसा, सत्य , ब्रह्रचार्य , अस्तेय , अपरिग्रह , शौच , संतोष , तप , स्वाध्याय , ईश्वर प्राणिधान उसके बाद यौगिक संस्थानों , पीठो तथा आश्रमों का निर्माण आरम्भ हुआ । जिनका मुख्य केन्द्र बिन्दू ाजयोग की शिक्षा व दीक्षा थी ।

श्रीमद्भगवतगीता में योग
भगवान श्री कृष्ण को आत्माराम ,परमयोगी की उपाधि से नवाजा गया है । श्रीमद्भगवतगीता में योग का वर्णन चार अध्यायों में किया गया है । अध्याय तीन में कर्मयोग के बारे में बताया गया है। जबकि छटे अध्याय में ध्यान योग का , बारहवें अध्याय में भक्तियोग और 15वें अध्याय में पुरषोत्तम योग का वर्णन किया गया है । आध्यात्मक दृष्टि से देखे तो इस योग साधना से निर्वाण और अध्यात्म उन्नति प्राप्त की जा सकती है ।
आयुर्वेद व योग का सामजंस्य
"आयुर्वेद का स्पष्ट प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं , आतुरस्य विकार प्रशमनं च " - इस वेद की उत्पत्ति ऋषिमुनियों ने अपने आध्यात्म यात्रा में आने वाली बाधाओं से निजात पाने के लिए की थी । ताकि आयुर्वेद से निरोगी रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके । शरीर शुद्वि के लिए आयुर्वेद में उल्लेखित क्रियाएं , आत्मा शुद्वि के लिए योग विद्या की क्रियाओं से समानता रखती है । जिस प्रकार आचार्य शार्गधर द्वारा शरीर शुद्वि के लिए पंच-कर्मों वमन, विरेचन ,निरूहण , अनुवासन तथा नस्य कर्म को निर्देश दिया गया है ।
उसी प्रकार हठ योग प्रदीपिका में योगियों को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए छह कर्मों धौति, बस्ति, नेति, त्राटक, नौलिका और कपालभाति का वर्णन किया हुआ है ।
आयुर्वेद के मूलभूत सिद्वातों के अनुसार वात, पित्त,कफ में से किसी एक की भी विकृति शारिरिक व मानसिक रोगों का कारण होती है । पतंजलि योग के अष्टाग योग के पहले तीन अंग - यम,नियम व आसन से इन तीन दोषों का संतुलन , समता होती है । यदि आयुर्वेद एक जीवन प्रणाली है, तो योग जीवन प्रबंधन हैं। आयुर्वेद प्रकृति का तंत्र है तो योग आत्मसाक्षात्कार का आध्यात्मिक दर्शन है ।
आधुनिक समय में योग की महता
भागमदौड की इस जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है । सबसे पहले सब कुछ पाने की दौड़ में इंसान इतना विचलित और असंतुलित हो चुका है । इससे बहार निकलने के लिए उसके पास एक ही विकल्प है । योग की शरण कहा जाता है कि" मन के हारे हार है , मन के जीते जीत " किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन की दृढ़ता और एकाग्रता जरूरी है ।
ये बात किसी से छुपी हुई नही है कि योग के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है । आज का इंसान नई-नई खोजें कर रहा है लेकिन जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है । उतनी ही तेजी से अपनी तरक्की में बाधा उत्पन करने वाले कारणो के प्रति भी सचेत हो रहा है ।
पूरे विश्व में आज योग का डंका बज रहा है । 21 जून को विश्वस्तर पर योग दिवस मनाया जाता है ।